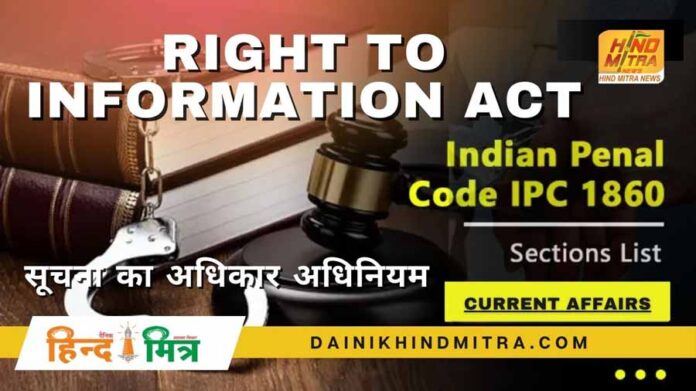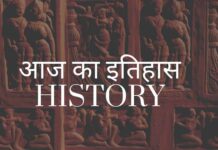Current Affairs | RTI Feature : सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जो भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के अनुसार, सभी को अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता है। सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय नागरिक के उस मौलिक अधिकार की रक्षा करता है।
आइये सूचना का अधिकार अधिनियम की मुख्य विशेषताओं तथा स्वयं अधिनियम पर करीब से नज़र डालें।
सूचना का अधिकार अधिनियम
RTI Feature : सूचना का अधिकार अधिनियम यूपीए सरकार द्वारा 11 मई 2005 को लोकसभा में तथा 12 मई 2005 को राज्यसभा में पारित किया गया था। काफी विचार-विमर्श के बाद 15 जून 2005 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस परियोजना को हरी झंडी दे दी गई। पारित होने के मात्र 120 दिन बाद ही 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हो गया।
सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोगों को सरकारी संगठनों सहित सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी मांगने का अधिकार है। कानून में नियम और प्रक्रियाएं बताई गई हैं कि कोई व्यक्ति किस तरह से जानकारी मांग सकता है। कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी दस्तावेज़ का अनुरोध कर सकता है और उसकी प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त कर सकता है।
अब, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 “सूचना” शब्द के अर्थ के बारे में क्या कहता है? इसके अनुसार, सूचना कई रूपों में आ सकती है, जैसे ज्ञापन और ईमेल, दस्तावेज़, प्रेस विज्ञप्तियाँ, राय, सलाह, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, रिपोर्ट, कागज़, नमूने, मॉडल और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहीत डेटा।
नागरिक आरटीआई अधिनियम के तहत इसका अनुरोध कर सकते हैं।
RTI Feature : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं
- आरटीआई अधिनियम लोगों को सरकारी दस्तावेजों को देखने और सरकार से कोई भी सार्वजनिक जानकारी मांगने की अनुमति देता है।
- सभी सरकारी निकाय, चाहे वे राज्य, केंद्र या स्थानीय हों, आरटीआई प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी हैं। सभी सरकारी स्वामित्व वाले संगठन भी आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं।
- आरटीआई प्रश्नों को संभालने के लिए एक जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) को नियुक्त किया जाएगा। यह व्यक्ति अनुरोध प्रपत्र स्वीकार करेगा और जनता को वह जानकारी देगा जो वे चाहते हैं।
- सहायक पीआईओ प्रत्येक जिला या संभागीय स्तर पर काम करते हैं और लोगों को सूचना प्राप्त करने में मदद करते हैं।
- आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को हिंदी या अंग्रेजी में आवेदन भरकर ईमेल से भेजना होगा। यदि आप इसे लिखकर नहीं भेज सकते हैं, तो पीआईओ आपके मौखिक अनुरोध को लिखित रूप में भेजने में सहायता करेंगे।
- यदि आवेदक बधिर, अंधा या विकलांग है, तो सार्वजनिक प्राधिकरण को सहायता प्रदान करनी होगी तथा मांगे गए दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करनी होगी।
- आवेदक को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि उन्हें सूचना क्यों चाहिए या कोई अन्य व्यक्तिगत जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है।
- यदि पीआईओ उसे समय पर आवश्यक सूचना नहीं देता है तो आवेदक उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है।
- विधान सभा को दी जाने वाली कोई भी सूचना आरटीआई अधिनियम के तहत किसी भी आवेदक को दी जानी चाहिए।
- आवेदक को अपेक्षित सूचना न देने पर पीआईओ को प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना देना होगा।
RTI Feature : आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा
आरटीआई अधिनियम की धारा 2(एच) बताती है कि सार्वजनिक प्राधिकरण क्या है।
एक “सार्वजनिक प्राधिकरण” कोई भी व्यक्ति या स्वशासन संस्था है जिसे स्थापित या गठित किया गया है:
- क) संविधान द्वारा या उसके कारण;
- ख) संसद द्वारा पारित किसी अन्य कानून द्वारा;
- ग) राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किसी अन्य कानून के परिणामस्वरूप; या
- घ) सरकारी अधिसूचना या आदेश द्वारा।
जो लोग चुनाव आयोग, केंद्र और राज्य सरकारों जैसे सरकारी निकायों तथा आरबीआई, सेबी और ट्राई जैसे नियामकों के लिए काम करते हैं, उन्हें सार्वजनिक निकाय कहा जाता है।
RTI Feature : सार्वजनिक प्राधिकरण कोई भी संगठन हो सकता है जिसका स्वामित्व, नियंत्रण या वित्तपोषण किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इसमें गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं जिन्हें सरकार से बड़ी मात्रा में धन मिलता है। इस भाग के बारे में बहस हुई है क्योंकि यह इस सवाल को खुला छोड़ देता है कि स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त वित्तपोषण का क्या मतलब है।
ऐसे सवालों ने इस अधिनियम की पारदर्शिता के बारे में बहुत सी चर्चाओं को जन्म दिया है। नतीजतन, इस शब्द का यह तत्व आरटीआई अधिनियम से संबंधित कई मामलों में इस्तेमाल किया जाता है।
यह भी देखें: Patrakarita: हिंदी पत्रकारिता का उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए
RTI Feature : सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य
सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना है।
RTI सबसे पहले कहाँ लागू हुआ ?
लंबी जद्दोजहद और मशक्कत के बाद 12 अक्टूबर 2005 को देश में सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ था। यह कानून स्वीडन में 1766 में लागू हो चुका था, वहीं भारत से पहले विश्व के 82 देशों में इस कानून का उपयोग किया जा रहा था।
RTI Feature : सूचना के अधिकार के दायरे में कौन कौन आता है ?
इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद व राज्य विधानमंडल के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) और निर्वाचन आयोग (Election Commission) जैसे संवैधानिक निकायों व उनसे संबंधित पदों को भी सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है।
सूचना के अधिकार (आरटीआई) के दायरे में कौन कौन नहीं आता है?
आरटीआई अधिनियम की धारा 24 में इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ आदि जैसे कुछ संस्थानों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन इनमें न्यायपालिका का कोई जिक्र नहीं है इसलिये न्यायपालिका को आरटीआई के दायरे में आना चाहिये।
RTI Feature : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 क्या है?
11. सूचना के लिए प्राप्त ऐसे आवेदन जिनकी सूचना अन्य लोक प्राधिकरण के द्वारा संधारित की जाती है, या जिनकी विषय वस्तु अन्य लोक प्राधिकरण के द्वारा किये जाने वाले कार्यो से संबंधित है, को आवेदन प्राप्ति के 5 दिवस में संबंधित लोक प्राधिकरण को स्थानान्तरित करना तथा इसकी सूचना आवेदक को देना
RTI Feature : भारत में आरटीआई का आविष्कार किसने किया था?
भारत में आरटीआई का विचार 1990 में पूर्व प्रधान मंत्री वीपी सिंह के दिमाग की उपज था। आरटीआई की शुरूआत के लिए पहला जमीनी स्तर का अभियान 1994 में मजदूर किसान शक्ति संगठन (एमकेएसएस) द्वारा शुरू किया गया था। पीपुल्स आरटीआई के लिए राष्ट्रीय अभियान – 1996 में गठित; सरकार के लिए आरटीआई कानून का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया।
सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में है?
संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत आरटीआई को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 19(1) के तहत हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे काम करती है, उसकी क्या भूमिका है, उसके क्या कार्य हैं आदि।
जिला सूचना अधिकारी कौन होता है?
लोक सूचना अधिकारी वह अधिकारी होता है जिन्हें सभी प्रशासनिक ईकाईयों या कार्यालयों में लोक अधिकारियों द्वारा आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त किया गया हो और उसे यह दायित्व दिया गया हो कि वे सूचना प्राप्ति के लिए आग्रह करने वाले सभी नागरिकों को सूचना प्रदान करेंगे।
RTI Feature : एक व्यक्ति एक वर्ष में कितनी बार आरटीआई के लिए आवेदन कर सकता है?
किसी भी निजी निकाय के लिए जो किसी भी अन्य कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा लागू किया जा सकता है. कितनी बार RTI को अप्लाई किया जा सकता है? एक ही संगठन में एक से अधिक RTI दर्ज करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है.
RTI Feature : सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है?
सूचना का अधिकार अधिनियम ‘ पारित करने वाले पहले राज्य तमिलनाडु और गोवा थे। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य था जिसने 1997 में तमिलनाडु सूचना का अधिकार कानून का उपयोग किया।
RTI का आवेदन कहाँ कहाँ किया जा सकता है?
सरकार की तरफ से सभी सार्वजनिक संस्थानों, विभाग, मंत्रालय में आरटीआई फाइल का जवाब देने के लिए लोक सूचना अधिकारी मौजूद होते हैं। आप केंद्र और राज्य सरकार के जिस विभाग के बारे में सूचना लेना चाहते हैं वहां के अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। आरटीआई फाइल करने के बाद 30 दिन के भीतर सरकार की तरफ से इसका जवाब देना अनिवार्य है।
प्रथम अपील क्या है?
प्रथम अपील के लिए कोई निश्चित प्रारूप (फॉर्म) नहीं होता है। आप चाहें तो एक सादे काग़ज़ पर भी लिखकर प्रथम अपील तैयार कर सकते हैं। हालांकि इस मामले में भी कुछ राज्य सरकारों ने प्रथम अपील के लिए एक ख़ास प्रारूप तैयार कर रखा है। प्रथम अपील आप डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से संबंधित कार्यालय में जाकर जमा करा सकते हैं।
प्रथम अपील की समय सीमा क्या है?
अपील दायर करने की समय-सीमा आवेदक द्वारा सूचना प्राप्त करने की तिथि की समाप्ति से या ऐसे निर्णय की प्राप्ति की तिथि से 30 दिन है।
सूचना का अधिकार में कुल कितनी धाराएं हैं?
अधिनियम की कुछ धाराएं नामत: धारा 4(10), 5(1) और (2), 12, 13, 15, 16, 24, 27 और 28 तत्काल प्रभाव से लागू हो गईं जो रिकार्ड/सूचना के रखरखाव और कंप्यूटरीकरण के लिए लोक प्राधिकारियों के उत्तरदायित्वों, लोक सूचना अधिकारी के पदनाम, केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के गठन, कुछ संगठनों को शामिल न करने आदि से संबंधित …
RTI के तहत कौन सी सूचना नहीं दी जा सकती?
(क) सूचना, जिसका प्रकटन भारत की सुरक्षा और अखण्डता को प्रभावित करेगा। (ख) न्यायालय द्वारा प्रकटन से वर्जित सूचना। (ग) सूचना, जिसका प्रकटन संसद/विधान सभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करेगा। (घ) वाणिज्यिक गोपनीयता से सम्बन्धित सूचना
यह भी देखें: Media Law and Ethics : मीडिया कानून और नैतिकता मूल सिद्धान्तों की जानकारी अनिवार्यतः होनी चाहिए
निष्कर्ष
सूचना का अधिकार अधिनियम की काफी आलोचना हुई है। उनका कहना है कि व्यवस्थागत खामियों के कारण यह अधिनियम अपने पूर्ण लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि आरटीआई अधिनियम के दुरुपयोग से उचित तरीके से निपटा जाना चाहिए, अन्यथा जनता का इस अधिनियम पर विश्वास और भरोसा खत्म हो जाएगा।
हालांकि, तथ्य यह है कि आरटीआई अधिनियम हमें यह देखने का दुर्लभ अवसर देता है कि सरकार किस प्रकार काम करती है, विशेष रूप से जमीनी स्तर पर, जहां नागरिकों की बात सबसे अधिक मायने रखती है कि काम कैसे किया जाए।